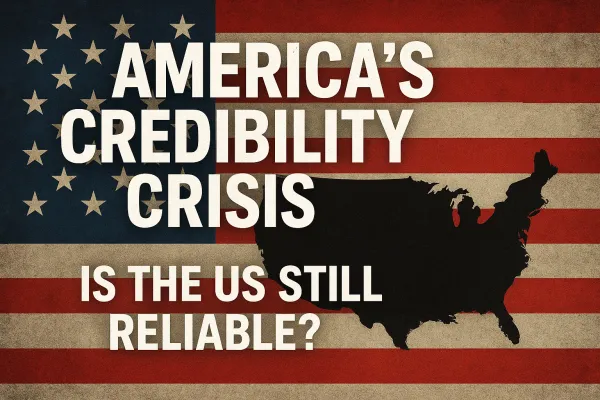द इंडो-पैसिफिक 2025: शक्ति, व्यावहारिकता और संतुलन की खोज
इंडो-पैसिफिक 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। यहां के देश अब अमेरिका या चीन का पक्ष चुनने के बजाय अपनी शर्तों पर कूटनीति कर रहे हैं। बहुध्रुवीय बहुलवाद, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और उभरती सुरक्षा वास्तुकला—2025 में वैश्विक शक्ति संतुलन का नया स्वरूप।

परिचय: इंडो-पैसिफिक क्यों महत्वपूर्ण है
आइए उस बात से शुरू करें जिसे अधिकांश समाचार कवरेज अनदेखा कर देती है: इंडो-पैसिफिक सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला एक और क्षेत्र नहीं है—यह मूल रूप से वह जगह है जहां 21वीं सदी का राजनीतिक और आर्थिक भविष्य लिखा जा रहा है। यह विशाल भौगोलिक विस्तार, अफ्रीका के पूर्वी तटरेखा से लेकर प्रशांत द्वीपों तक फैला हुआ है, जिसमें दुनिया की आधी से अधिक आबादी रहती है और वैश्विक आर्थिक विकास का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्पन्न करती है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार का लगभग 70% इन जलमार्गों से होता है, जिसमें फारस की खाड़ी के तेल से लेकर वियतनामी इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ शामिल है।
2025 को विशेष रूप से दिलचस्प बनाने वाली बात केवल ये प्रभावशाली आंकड़े नहीं हैं। असली बदलाव यह है कि इस क्षेत्र के देश अमेरिका या चीन—किसी एक पक्ष को चुनने की पुरानी रणनीति को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। इसके बजाय, वे शक्ति राजनीति के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण तैयार कर रहे हैं जो गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के बारे में दशकों की पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं।
द्विआधारी प्रतिद्वंद्विता से आगे बढ़ना: बहुध्रुवीय बहुलवाद का उदय
वर्षों से, विश्लेषकों ने इंडो-पैसिफिक का वर्णन मुख्य रूप से एक लेंस के माध्यम से किया: अमेरिकी नेतृत्व चीनी विस्तार का सामना कर रहा है। वह ढांचा हमेशा अति सरलीकृत था, लेकिन 2025 तक जमीन पर वास्तव में क्या हो रहा है, यह समझने के लिए लगभग बेकार हो गया है।
इस साल के सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग को लें। जबकि अमेरिकी और चीनी अधिकारियों ने नियम-आधारित व्यवस्था बनाम संप्रभुता के बारे में अपने अनुमानित भाषण दिए, वास्तविक बातचीत साइड मीटिंग्स में हुई जहां दक्षिण पूर्व एशियाई राजनयिकों ने अपनी स्थिति स्पष्ट की: हम आपकी टीम नहीं चुन रहे हैं। इंडोनेशिया बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के साथ संबंध बना रहा है। वियतनाम भी यही कर रहा है। सिंगापुर जहां भी रणनीतिक अर्थ रखता है, वहां साझेदारी बना रहा है। यह तटस्थता या अनिर्णय नहीं है—यह विकल्पों को अधिकतम करने और संप्रभुता बनाए रखने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कूटनीति है।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन ने इस बदलाव को तब पकड़ा जब उन्होंने इंडो-पैसिफिक को सिर्फ एक और अमेरिका-चीन युद्धक्षेत्र के रूप में चित्रित करने को अस्वीकार कर दिया, इसके बजाय रणनीतिक स्वायत्तता की मांग की। वह संदेश ठीक इसलिए गूंजा क्योंकि यह उस चीज़ को दर्शाता है जो क्षेत्रीय अभिनेता पहले से ही अभ्यास करते हैं: विविध संबंध बनाए रखना जो उनके हितों की सेवा करते हैं बजाय द्विआधारी विकल्पों को मजबूर करने के।
संयुक्त राज्य अमेरिका: वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच रणनीतिक पुनर्गठन
अमेरिका इंडो-पैसिफिक में गहराई से लगा हुआ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप के दूसरे प्रशासन के तहत दृष्टिकोण बदल गया है। अमेरिकी नौसेना अभी भी नौवहन की स्वतंत्रता से जुड़े अभियान चलाती है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड साझेदारी भी जारी है। लेकिन अब हर चीज़ में अधिक लेन-देन वाला नज़रिया दिखता है—सुरक्षा खर्च में भार-साझाकरण पर अधिक जोर, लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं के लिए कम धैर्य, और ऐसी व्यापार नीतियां जो कभी-कभी उन्हीं सहयोगियों के साथ तनाव पैदा करती हैं जिनका वाशिंगटन समर्थन करने का दावा करता है।
भारत अमेरिकी रणनीति के लिए बिल्कुल केंद्र बन गया है। यह तर्क समझ में आता है: बढ़ती सैन्य क्षमताओं और एक विशाल अर्थव्यवस्था के साथ एक लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में, भारत उन तरीकों से चीन को संतुलित कर सकता है जो अकेले अमेरिकी बल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जटिलता तस्वीर में प्रवेश करती है। भारत इस साझेदारी का स्वागत करता है लेकिन अपनी शर्तों पर जोर देता है। नई दिल्ली बहुत अच्छी तरह से याद करती है कि पश्चिमी सहयोगी पिछले संकटों में कैसे अविश्वसनीय साबित हुए, और यह किसी के जूनियर पार्टनर बनने के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए दृढ़ है।
यह एक दिलचस्प नृत्य बनाता है। वाशिंगटन को भारत की ज़रूरत शायद उससे अधिक है जितना वह स्वीकार करना चाहता है, जबकि भारत इस पर निर्भरता चाहे बिना अमेरिकी समर्थन से लाभान्वित होता है।
चीन: मुखर विस्तार और आर्थिक कूटनीति
चीन की इंडो-पैसिफिक रणनीति आर्थिक प्रलोभन को सैन्य दावे के साथ उन तरीकों से मिश्रित करती है जो पड़ोसियों को आकर्षित और चिंतित दोनों करती है। बेल्ट एंड रोड पहल ने दर्जनों देशों में बंदरगाहों, राजमार्गों और डिजिटल बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित किया है, जिससे आर्थिक संबंध बनते हैं जिनका बीजिंग राजनीतिक प्रभाव के लिए लाभ उठाता है। दक्षिण चीन सागर में, चीन अब जरा सा भी परेशान नहीं हो रहा है—सैन्यीकृत कृत्रिम द्वीप, आक्रामक तटरक्षक संचालन, और क्षेत्रीय दावे जो पड़ोसियों को तेजी से चिंतित कर रहे हैं।
फिर भी चीन को ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो इन महत्वाकांक्षाओं को जटिल बनाती हैं। आर्थिक विकास काफी धीमा हो गया है। जनसांख्यिकीय रुझान प्रतिकूल हैं—कामकाजी उम्र की आबादी सिकुड़ रही है। और कुछ बीआरआई परियोजनाओं ने गंभीर प्रतिक्रिया उत्पन्न की है जहां वादा किए गए लाभ ऋण बोझ में बदल गए। बीजिंग ऊर्जा आयात और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ रहता है, लेकिन आगे का रास्ता आत्मविश्वासपूर्ण बयानबाजी की तुलना में अधिक जटिल है।
भारत: रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय नेतृत्व
यदि एक देश है जिसकी इंडो-पैसिफिक प्रक्षेपवक्र विधिपूर्वक ध्यान देने योग्य है, तो वह भारत है। नई दिल्ली ने बहुत तेजी से नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार किया है, खुद को प्रमुख हिंद महासागर शक्ति के रूप में स्थापित करते हुए जापानी, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से पूर्व की ओर संचालन का विस्तार कर रहा है।
भारत के दृष्टिकोण को विशिष्ट बनाने वाली सावधानीपूर्वक संतुलन अधिनियम है। यह क्वाड में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह आसियान के साथ गहराई से जुड़ता है। यह रूस के साथ रक्षा सहयोग बनाए रखता है। यह एक तनावपूर्ण सीमा टकराव का प्रबंधन करने के बावजूद चीन के साथ भारी व्यापार करता है। यह भ्रम नहीं है—यह भारत के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई गणनात्मक रणनीति है, बिना किसी एकल साझेदार पर विकल्पों को बंद करने या निर्भरता स्वीकार करने के।
भारतीय नीति निर्माता इसे रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, जिसका अर्थ है घटनाओं को आकार देने के लिए पर्याप्त क्षमता और संबंध होना बजाय केवल दूसरों द्वारा किए गए विकल्पों पर प्रतिक्रिया देने के। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और भारत इसे प्राप्त करने के लिए खुद को स्थापित कर रहा है।
मध्य शक्तियां और यूरोप का बढ़ता प्रभाव
जापान और ऑस्ट्रेलिया महाशक्ति संसाधनों की कमी के बावजूद क्षेत्रीय स्थिरता में काफी योगदान देते हैं। दोनों नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के चैंपियन हैं, प्रशांत द्वीप साझेदारी में निवेश करते हैं, और चीनी परियोजनाओं के बुनियादी ढांचा विकल्पों का समर्थन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच AUKUS साझेदारी सुरक्षा वास्तुकला में एक और परत जोड़ती है जो कुछ साल पहले मौजूद नहीं थी।
इस बीच, यूरोपीय जुड़ाव उन तरीकों से बढ़ा है जो उन लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है जो इंडो-पैसिफिक को विशुद्ध रूप से एशियाई-अमेरिकी इलाके के रूप में सोचते हैं। फ्रांस और यूके वहां क्षेत्र बनाए रखते हैं और नियमित रूप से नौसैनिक उपकरण तैनात करते हैं। ईयू जलवायु साझेदारी और व्यापार समझौतों का पीछा करता है जो क्षेत्रीय चर्चाओं में बहुपक्षवाद और विनियमन पर विभिन्न दृष्टिकोण लाते हैं। यह यूरोपीय भागीदारी राजनयिक विकल्पों में विविधता लाती है और उपयोगी तरीकों से शक्ति गणना को जटिल बनाती है।
उभरती सुरक्षा वास्तुकला
इंडो-पैसिफिक सुरक्षा बातचीत पारंपरिक सैन्य चिंताओं से कहीं आगे बढ़ गई है। जलवायु भेद्यता, साइबर खतरे, आपूर्ति श्रृंखला नाजुकता, और महामारी की तैयारी अब रणनीतिक योजना में नौसैनिक निर्माण और क्षेत्रीय विवादों के साथ समान स्थान पर हैं। इस साल के स्टेट ऑफ द इंडो-पैसिफिक सम्मेलन ने टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों के माध्यम से आर्थिक जबरदस्ती को पारंपरिक सैन्य खतरों के समान ध्यान देने योग्य सुरक्षा चुनौतियों के रूप में उजागर किया।
नई संस्थागत अवधारणाएं उभर रही हैं, जैसे इंडो-पैसिफिक संधि संगठन के प्रस्ताव जो राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए सहयोग तंत्र को औपचारिक बनाएंगे। ये विचार प्रारंभिक चरण में हैं, लेकिन वे व्यापक मान्यता का संकेत देते हैं कि मौजूदा ढांचे समकालीन चुनौतियों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं।
निष्कर्ष: एक स्थायी इंडो-पैसिफिक व्यवस्था के लिए जटिलता को गले लगाना
2025 में इंडो-पैसिफिक सरलीकरण से इनकार करता है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता नहीं है, हालांकि वह प्रतिस्पर्धा लगभग सब कुछ आकार देती है। यह साफ-साफ प्रतिस्पर्धी गुटों में विभाजित नहीं है, हालांकि गठबंधन निश्चित रूप से मौजूद हैं। इसके बजाय, जो हम देख रहे हैं वह एक तरल, बहुध्रुवीय वातावरण है जहां राज्य वास्तविक एजेंसी का प्रयोग करते हैं और विशिष्ट हितों और मूल्यों के आधार पर चयनात्मक साझेदारी बनाते हैं।
इस वातावरण में सफलता के लिए द्विआधारी सोच को त्यागने की आवश्यकता है। यह क्षेत्रीय नेताओं की स्वायत्तता का सम्मान करने की मांग करता है बजाय उन्हें किसी और के शतरंज की बिसात पर टुकड़ों के रूप में व्यवहार करने के। यह सैन्य तैयारी के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की आवश्यकता है। सबसे मौलिक रूप से, यह मान्यता की आवश्यकता है कि इंडो-पैसिफिक का भविष्य किसी एकल शक्ति द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा बल्कि दर्जनों राष्ट्रों द्वारा सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच लगातार नेविगेट करने से होगा।
वह नेविगेशन क्षेत्र से परे मायने रखता है। इंडो-पैसिफिक देश इन तनावों को कैसे प्रबंधित करते हैं, वैश्विक शासन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पैटर्न, और आने वाले दशकों के लिए महान-शक्ति संबंधों को आकार देगा। इस जटिलता को समझना केवल शैक्षणिक रुचि नहीं है—यह किसी के लिए भी आवश्यक है जो यह समझना चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आने वाले वर्षों में कहां जा रही है।
संबंधित लेख:
- भारत का रणनीतिक संतुलन नीति 2025: अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों का प्रबंधन और घरेलू राजनीति का इसके विदेश नीति पर असर।
- टैरिफ शॉक 2.0: क्यों अमेरिका-चीन नियंत्रण वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से आकार दे रहे हैं — अमेरिका-चीन टैरिफ और निर्यात नियंत्रण से लागत बढ़ना, चिप्स और खनिजों की आपूर्ति सीमित होना, और सप्लाई चेन में बदलाव। महंगाई, तकनीक पहुंच और रणनीति पर असर।
- ट्रम्प का दावा बनाम भारत की तेल वास्तविकता: — क्या नई दिल्ली रूसी तेल बंद करेगी या समझदारी से विविधीकरण बढ़ाएगी? सस्ती कीमत, आपूर्ति सुरक्षा और कूटनीति का संतुलन।
- अमेरिका की ऊर्जा और जलवायु कूटनीति: अमेरिका कैसे ऊर्जा और जलवायु को वैश्विक प्रभाव के लिए इस्तेमाल करता है, और भारत के दृष्टिकोण के लिए संदर्भ।
- 2025 रूस-यूक्रेन युद्ध का विश्लेषण: नाटो, ट्रम्प: नाटो की भूमिका, ट्रंप और आगे के संभावित परिदृश्य—वैश्विक भू-राजनीति का भारत पर प्रभाव।
लेख पसंद आया?
हमारे मुख्य पृष्ठ पर जाएं और नई जानकारियों व अपडेट्स के लिए सदस्यता लें!