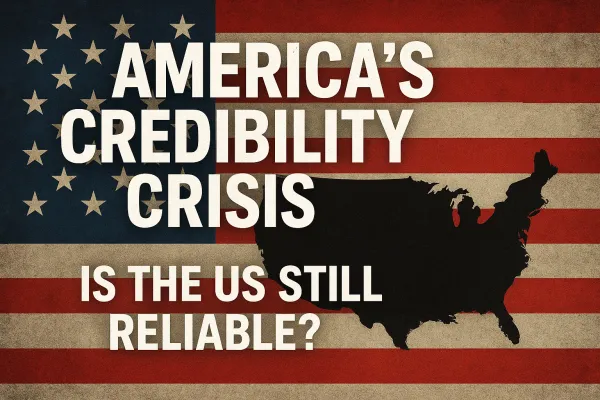बदलता भारतीय लोकतंत्र 2025: शासन, विपक्ष और जनता की सोच
भारतीय लोकतंत्र अब डिजिटल, केंद्रित और परिणाम-उन्मुख है। विपक्ष और जनता की बदलती भूमिका को समझें।

भारतीय लोकतंत्र कभी भी बोरिंग नहीं रहा। ये हमेशा से एक अजीब, अप्रत्याशित चीज रही है जो किसी तरह चलती रहती है, भले ही सब इसके खिलाफ दांव लगाते रहें। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ बदला है। रातोंरात क्रांति वाली बात नहीं, बल्कि इतनी धीरे-धीरे कि आप नोटिस भी नहीं करते जब तक पीछे मुड़कर न देखें।
अब सरकारें जिस तरह से काम करती हैं, विपक्षी पार्टियां जिस तरह (अक्सर नाकाम होते हुए)
प्रासंगिक बने रहने की कोशिश करती हैं, और आम लोग वोट डालते वक्त क्या उम्मीद रखते हैं—ये सब दस साल पहले से काफी अलग दिखता है। से समझना जरूरी है, इसलिए नहीं कि सब अच्छा या बुरा है, बल्कि इसलिए कि हम सब इसी दौर में जी रहे हैं।
डिजिटल गवर्नेंस की क्रांति
लाइनों से लेकर ऐप्स तक
याद है जब सरकारी काम कराने के लिए पूरा दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी? किसी ऑफिस जाना, घंटों लाइन में खड़े रहना, किसी क्लर्क की मूड पर निर्भर करना कि काम होगा या नहीं, और कभी-कभी रिश्वत देकर काम "स्पीड अप" करना। यह बस दस साल पहले की बात है।
आज स्थिति बदल गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में खेती करने वाले किसान को सब्सिडी का पैसा सीधे उसके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई क्लर्क नहीं, कोई रिश्वत नहीं। गांव छोड़कर जाने की जरूरत भी नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अब तक करीब 35 लाख करोड़ रुपये सीधे नागरिकों तक पहुंचे हैं। यह छोटा बदलाव नहीं है—यह नागरिक और सरकार के बीच संपर्क का पूरा रूप बदल रहा है।
और बात केवल पैसे ट्रांसफर तक सीमित नहीं है। UPI ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स में अग्रणी बना दिया (जो सच में किसी ने सोचा भी नहीं था)। डिजिटल लॉकर में दस्तावेज़ सुरक्षित हैं, आधार कार्ड से पहचान होती है, और टैक्स फाइल करने से लेकर राशन कार्ड की स्थिति चेक करने तक—हर चीज के लिए ऐप्स मौजूद हैं।
इस बदलाव का असली मतलब क्या है
बात सिर्फ सुविधा की नहीं है। जब पैसा पार्टी कार्यकर्ता या स्थानीय अफसरों के बजाय सीधे लोगों तक पहुँचने लगता है, तो मूल रूप से यह तय करता है कि सत्ता किसके पास है। पुराना सिस्टम संरक्षण (patronage) पर चलता था। आपको किसी को जानना पड़ता था, किसी नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ता था, और सही समुदाय या पार्टी से जुड़े रहना पड़ता था। डिजिटल ट्रांसफर ने यह पूरा खेल ही बदल दिया।
क्या इससे भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया? शायद नहीं। लेकिन खेल ज़रूर बदल गया है। साथ ही यह कहना भी जरूरी है—जब सरकार के पास नागरिकों का इतना बड़ा डेटा होता है, तो गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और डिजिटल असमानता जैसे सवाल स्वाभाविक हैं। जिनके पास स्मार्टफोन या स्थिर इंटरनेट नहीं है, वे पीछे रह सकते हैं। हर प्रणाली की तरह, यह भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बदलाव की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसके साथ ही अब शासन व्यवस्था में “मिशन मोड” की सोच तेज़ी से बढ़ रही है। बड़े सरकारी कार्यक्रम तय समय सीमा और लगातार निगरानी के साथ चलाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, और बुनियादी ढाँचे से जुड़े प्रोजेक्ट—ये सभी ऊपर से नीचे तक सख़्त लक्ष्य तय करके आगे बढ़ाए जाते हैं।
इससे काम में गति आती है, लेकिन एक सवाल उठता है—क्या इससे स्थानीय स्तर पर लचीलापन और जवाबदेही कम हो रही है?
जिन समझौतों पर कोई बात नहीं करता
क्या इस तरीके से काम जल्दी होता है? ज़्यादातर मामलों में, हाँ।
क्या कभी-कभी यह नज़रअंदाज़ कर देता है कि हर राज्य की ज़रूरतें अलग होती हैं? यह भी सच है।
असली खींचतान है — कार्यक्षमता बनाम लचीलापन, गति बनाम स्थानीय अनुकूलन।
हर व्यक्ति इन बातों को अलग नज़रिए से देखेगा, इस पर निर्भर करता है कि वह किस जगह खड़ा है और किस अनुभव से गुजर रहा है।
समस्या तब होती है जब लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई समझौते हैं ही नहीं।
डिजिटल शासन ने बहुत सी चीज़ें बेहतर बनाई हैं, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं।
दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं — और यही समझ परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है।
विपक्ष की लगातार दुविधा
राज्य बनाम राष्ट्रीय विरोधाभास
विपक्ष आज एक अजीब स्थिति में है। राज्य स्तर पर कई पार्टियां मजबूत हैं—DMK तमिलनाडु में, तृणमूल बंगाल में, कांग्रेस कुछ राज्यों में। क्षेत्रीय दल अपने इलाकों में असर बनाए हुए हैं।
लेकिन जब बात राष्ट्रीय राजनीति की आती है, तो यही ताकत बिखर जाती है।
यह सिर्फ नेतृत्व की कमी नहीं है—मुद्दा और गहरा है, एक साझा दिशा और ठोस रणनीति का अभाव।
सिर्फ नेतृत्व से आगे की समस्या
असल मुद्दा और गहरा है। जब पूरी राजनीति “कितने घर बने, कितने शौचालय बने, कितना तेज़ काम हुआ” जैसे नतीजों पर टिकी हो, तो विपक्ष का जवाब क्या हो सकता है? यह कहना आसान है कि क्या ठीक से नहीं हुआ—पर उसके बाद क्या? लोगों को एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता दिखाना होगा, जिस पर वे भरोसा कर सकें। सिर्फ आलोचना काफी नहीं है। हर कोई सवाल कर सकता है लेकिन शासन चलाने या उसका भरोसेमंद विकल्प पेश करने की क्षमता दिखाना — वही असली चुनौती है।
गठबंधन की उलझन
विपक्षी पार्टियों का पूरा दृश्य कभी-कभी बहुत जटिल लगता है। हर कुछ महीने में हम सुनते हैं कि पार्टियां एकजुट हो रही हैं, गठबंधन बन रहे हैं—और फिर वही पुराने मतभेद सामने आ जाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों पर ध्यान देती हैं (जो समझ आता है—वहीं उनकी असली ताकत है), जबकि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय अक्सर पीछे रह जाता है।
इसमें आर्थिक नीतियों, सामाजिक मुद्दों और शासन के दृष्टिकोण पर असली विचारधारात्मक मतभेद भी जुड़ जाते हैं, और आपको अस्थिरता का पूरा मिश्रण मिल जाता है।
कुछ प्रयास जरूर हुए हैं—जैसे INDIA गठबंधन ने कुछ मुद्दों पर तालमेल बनाने की कोशिश की। लेकिन स्पष्ट नेतृत्व और एकजुट संदेश के साथ स्थायी सहयोग अभी भी गायब है।
डिजिटल संचार में कमजोरी
ज्यादातर विपक्षी पार्टियां डिजिटल कम्युनिकेशन में पीछे हैं। जबकि सत्तारूढ़ पार्टी समझ चुकी है कि अब वोटर्स तक पहुँचने का सबसे असरदार तरीका उनके फोन और सोशल मीडिया के जरिए है—मन की बात, डायरेक्ट सोशल मीडिया, ऐप्स, और टारगेटेड मैसेजिंग।
विपक्ष अब भी 2010 की तरह काम करता है—प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, शायद ट्वीट करेगा, और आश्चर्य करेगा कि कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा। जब आपका प्रतिद्वंद्वी सीधे लाखों लोगों तक पहुँच रहा है, और आप जर्नलिस्ट्स का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपके बयान कवर करें, तो आधी जंग आप पहले ही हार चुके हैं।
विपक्ष अभी खत्म नहीं हुआ
लेकिन विपक्ष को पूरी तरह ख़ारिज करना जल्दबाजी होगी। भारतीय राजनीति हमेशा उतार-चढ़ाव भरी रही है। जो पार्टियां अजेय लगती थीं, अचानक हार सकती हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं—ये अपने आप गायब नहीं होतीं। और क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे उनकी राष्ट्रीय समन्वय की कमजोरियाँ कुछ भी हों, अपने राज्यों में मजबूत बनी रहती हैं।
विपक्ष के लिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या वे सरकार की आलोचना कर सकते हैं। कोई भी शिकायत कर सकता है। असली चुनौती यह है कि क्या वे वोटर्स को विश्वास दिला सकें कि उनका विकल्प भरोसेमंद और क्रियाशील है। जब तक वे इसे नहीं समझतीं, वे कुछ राज्यों में जीत सकती हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संघर्षरत रहेंगी।
जनता की धारणा: भारतीय लोकतंत्र से क्या चाहते हैं
प्रदर्शन की उम्मीद
अब वोटर्स वास्तव में क्या चाहते हैं? यह काफी बदल गया है। खासकर युवा वोटर्स, वे सरकारों को सिर्फ वादों या विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि असली, ठोस नतीजों के आधार पर आंक रहे हैं।
विचारधारा मर गई है ऐसा नहीं है, लेकिन अब इसमें कुशल और असरदार शासन की उम्मीदें भी शामिल हो गई हैं। अपने सिद्धांतों की बातें करना अब काफी नहीं है—आपको दिखाना होगा कि आप काम को प्रभावी ढंग से चला सकते हैं।
नंबर क्या दिखाते हैं
सर्वे डेटा बताते हैं कि लोग सबसे ज्यादा नौकरी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। साथ ही, वे राजनीतिक ढंग से समझदार भी हैं। भारत में वोटर टर्नआउट अक्सर पश्चिमी लोकतंत्रों से भी बेहतर होता है। लोग राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अलग तरीके से वोट करते हैं, जो दिखाता है कि वे सरकार के अलग-अलग स्तर और जिम्मेदारियों को समझते हैं। ये लो-इनफॉर्मेशन वोटिंग नहीं है, बल्कि काफी सूक्ष्म राजनीतिक सोच है।
सोशल मीडिया का असर
सोशल मीडिया ने राजनीतिक बातचीत का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब किसी अखबार या टीवी एडिटर का इंतजार करना जरूरी नहीं कि वो तय करें क्या महत्वपूर्ण है। बहसें WhatsApp ग्रुप्स और Twitter थ्रेड्स में होती हैं।
लेकिन इसके साथ ही इको चैंबर और फेक न्यूज़ की समस्या भी बढ़ी है। वही प्लेटफॉर्म जो जानकारी फैलाते हैं, वही लोगों को प्रभावित और भ्रमित करना भी आसान बनाते हैं।
युवा कारक
युवा वोटर्स अलग हैं। वे राजनीति को ज्यादातर फोन और सोशल मीडिया के जरिए समझते हैं—इन्फ्लुएंसर्स और मीम्स के माध्यम से। वे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं—जैसे जलवायु परिवर्तन, लिंग समानता और जवाबदेह शासन। उनके पास उन नेताओं के लिए कम धैर्य है जो सिर्फ भाषण देते हैं और कुछ नहीं करते।
लेकिन वे ध्रुवीकृत नैरेटिव और दिखावटी राजनीति के लिए भी अधिक संवेदनशील हैं।
संस्थानों में विश्वास
भारतीय अभी भी ज्यादातर चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि वोट गिना जाता है और चुनाव निष्पक्ष होते हैं।
लेकिन अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों—मीडिया, न्यायपालिका, संसद—में विश्वास कहीं अधिक अस्थिर है। यह दिखाता है कि लोग लोकतंत्र को एक पूरी इकाई के बजाय विभिन्न संस्थाओं का संग्रह मानते हैं और हर एक को अलग से जज करते हैं।
तीनों का संगम: गवर्नेंस, विपक्ष और जनता
गवर्नेंस राजनीति को कैसे आकार देती है
गवर्नेंस, विपक्ष और जनता की धारणा—ये तीनों आपस में जुड़े हैं। जब सरकार कुशलतापूर्वक लाभ लोगों तक पहुंचाती है, तो यह तय करती है कि लोग राजनीति को कैसे देखें। और यह विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर करता है। अब आप सिर्फ “भ्रष्टाचार” की बातें नहीं कर सकते, जब सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंच रही है।
कमजोर विपक्ष सबके लिए चिंता का विषय
कमजोर विपक्ष सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी चुनौती है। मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है—पॉलिसी की जांच, असफलताओं को उजागर करने और वैकल्पिक रास्ते पेश करने के लिए। जब विपक्ष टूटा और कम प्रभावशाली होता है, तो सरकारी कार्रवाइयों की निगरानी कम होती है, संसद में बहस कमजोर होती है, और कार्यपालिका पर कम नियंत्रण रहता है।
यह हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी पार्टी को समर्थन दें। लोकतंत्र के लिए क्रियाशील विपक्ष होना जरूरी है।
धारणा की लड़ाई
अंततः, जनता की धारणा चुनावों को आकार देती है। यदि लोग महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो वे वर्तमान सरकार को इनाम देते हैं। अगर वे पीछे छूटे महसूस करते हैं, तो वे वैकल्पिक विकल्प खोजते हैं।
लेकिन यह धारणा केवल वास्तविक अनुभव से नहीं बनती। यह जाति, समुदाय और सोशल मीडिया/WhatsApp पर डोमिनेंट नैरेटिव्स से भी प्रभावित होती है। यही है लोकतंत्र की जटिल और वास्तविक दुनिया—जो कभी साफ-सुथरी नहीं, बल्कि अक्सर उलझी हुई होती है।
चुनौतियां और अवसर
डिजिटल डिवाइड का सवाल
सबसे बड़ी चुनौती यह है कि डिजिटल शासन किसी को पीछे न छोड़ दे। तकनीक का लाभ सभी तक पहुँचना चाहिए—स्मार्टफोन और इंटरनेट वाले और बिना इंटरनेट वाले लोगों के बीच नई खाई न बने। यह केवल अच्छा विचार नहीं, बल्कि जरूरी है यदि हम इस तरीके को गंभीरता से अपनाना चाहते हैं।
मजबूत विपक्ष की आवश्यकता
क्या हम एक मजबूत विपक्ष बना सकते हैं? केवल वे पार्टियाँ नहीं जो कभी-कभार राज्य चुनाव जीत सकें, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद विकल्प प्रस्तुत करें। लोकतंत्र में जनता के पास वास्तविक विकल्प होना जरूरी है। अभी यह विकल्प सीमित सा लगता है।
सूचना और गलत जानकारी
पूरे सूचना तंत्र पर ध्यान देना जरूरी है। गलत और झूठी जानकारी से लड़ते हुए, हम लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रखें? आज के समय में, लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना और उन्हें समझना लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
संघीय बनाम केंद्रीय
केंद्रीय और राज्य शासन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। राष्ट्रीय कार्यक्रम तो चलाएँ, लेकिन राज्यों की आवश्यकताओं और विविधता का सम्मान भी होना चाहिए। भारत हमेशा विविध रहा है—भाषा, संस्कृति और समस्याओं में। सभी के लिए एक ही तरीका यहाँ कभी पूरी तरह काम नहीं कर सकता।
चुनावों से परे
लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका, मीडिया, संसद, प्रशासन और समाजिक संगठन—इन सभी की स्वतंत्रता और ताकत जरूरी है। केवल चुनाव से ही मजबूत लोकतंत्र नहीं बनता। इन सभी संस्थाओं को निरंतर ध्यान और सुधार की आवश्यकता है।
निष्कर्ष: गतिशील और बदलता लोकतंत्र
तो क्या भारतीय लोकतंत्र कम लोकतांत्रिक हो रहा है? हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन यह निश्चित रूप से बदल रहा है। शासन अब ज्यादा डिजिटल, ज्यादा केंद्रीकृत और नतीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। विपक्षी राजनीति नेशनल स्तर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि कई राज्यों में सफल है। नागरिक अब ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही ज्यादा विभाजित भी हैं, और वे प्रदर्शन और प्रतिनिधित्व दोनों की उम्मीद रखते हैं।
इन बदलावों में से कोई भी भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को तय नहीं करता। लोकतंत्र कोई अंतिम मंजिल नहीं है—यह एक प्रक्रिया है। यह उलझा हुआ, विवादास्पद और हमेशा बदलते रहने वाला है। सवाल यह नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र परफेक्ट है या नहीं—क्योंकि कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता। सवाल यह है कि क्या यह खुद को सुधार सकता है, क्या संस्थान मजबूत और सक्षम बन सकते हैं, और क्या नागरिक जुड़ाव और जानकारी के साथ रहते हैं।
हम जो देखते हैं, वह है प्रगति और समस्याएँ। उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ—दोनों मौजूद हैं। कोई भी यह नहीं बता सकता कि सब ठीक चल रहा है या सब गिर रहा है, यह बहुत सरलीकरण होगा। असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल और रोचक है।
भारतीय लोकतंत्र की कहानी अभी लिखी जा रही है। एक अरब से अधिक लोग इसे मिलकर लिख रहे हैं—अपने वोटों, अपनी आवाज़ और अपने दृष्टिकोण के जरिए कि भारत कैसा होना चाहिए। इस पर ध्यान देना जरूरी है, चाहे आपकी राजनीति कुछ भी हो।
संबंधित लेख:
- भारत का रणनीतिक संतुलन नीति 2025: अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों का प्रबंधन और घरेलू राजनीति का इसके विदेश नीति पर असर।
- 2025 रूस-यूक्रेन युद्ध का विश्लेषण: नाटो, ट्रम्प: नाटो की भूमिका, ट्रंप और आगे के संभावित परिदृश्य—वैश्विक भू-राजनीति का भारत पर प्रभाव।
- अमेरिका की ऊर्जा और जलवायु कूटनीति: अमेरिका कैसे ऊर्जा और जलवायु को वैश्विक प्रभाव के लिए इस्तेमाल करता है, और भारत के दृष्टिकोण के लिए संदर्भ।
लेख पसंद आया?
हमारे मुख्य पृष्ठ पर जाएं और नई जानकारियों व अपडेट्स के लिए सदस्यता लें!