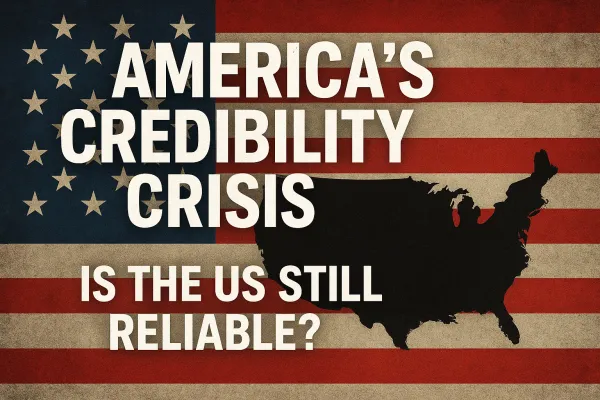सहयोगियों से प्रतिद्वंद्वी तक: तालिबान–पाकिस्तान संबंधों का टूटना और दक्षिण एशिया पर इसका प्रभाव
अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान के संबंधों और रणनीति का विश्लेषण, और यह दक्षिण एशिया की सुरक्षा और भारत की भूमिका को कैसे प्रभावित करता है।

पाकिस्तान की रणनीतिक भूल और उसका चक्रव्यूह
जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया, पाकिस्तान की सत्ता के केंद्र में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान के लिए यह दशकों से चली आ रही रणनीति की अंतिम सफलता जैसी थी। उन्होंने दशकों से तालिबान को आश्रय, प्रशिक्षण और राजनीतिक समर्थन दिया था, और इस्लामाबाद को लगा था कि उनका लंबा निवेश फल देगा — काबुल में एक मित्रवत शासन पाकिस्तान के हितों के अनुरूप काम करेगा।
लेकिन चार साल बाद, वह सपना समस्या में बदल गया है। वही समूह जिसे पाकिस्तान ने कभी समर्थन दिया, अब सीमा पार से उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। तनाव बढ़ गए हैं, सीमा पर झड़पें आम हो गई हैं, और पाकिस्तान की वह “रणनीतिक गहराई” जो वह चाहता था, अब एक बड़ा संकट बन गई है। यह पूरी स्थिति दिखाती है कि पाकिस्तान की अफगान नीति कितनी दृष्टिहीन थी और क्षेत्रीय लाभ के लिए विचारधारा और प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल करने के खतरे कितने गंभीर हैं।
पाकिस्तान की तालिबान रणनीति की जड़ें: प्रॉक्सी युद्ध का इतिहास
हथियारबंद समूहों के प्रति पाकिस्तान का दशकों पुराना समर्थन
पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता कभी भी धार्मिक आस्था या भाईचारे पर आधारित नहीं था — यह एक ठंडी और गणनात्मक भू-राजनीतिक चाल थी, जो सैन्य जुनून और गलत रणनीति से प्रेरित थी।
- भारत के खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी बनाना: वर्षों तक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अफगानिस्तान को एक तरह का पिछलग्गू मानती थीं — ऐसा क्षेत्र जो भारत के साथ संघर्ष में “रणनीतिक गहराई” प्रदान कर सके। इस दृष्टिकोण ने अफगान मामलों में लगातार हस्तक्षेप को जन्म दिया, जो अक्सर क्षेत्रीय शांति और अफगान संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता था।
- भारतीय प्रभाव को रोकना: कोई भी अफगान सरकार जो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की कोशिश करती, खासकर भारत के साथ मित्रवत संबंध, उसे रावलपिंडी में खतरे के रूप में देखा जाता। कूटनीति या व्यापार के बजाय, पाकिस्तान ने उन समूहों को समर्थन दिया जो काबुल को भारत की ओर झुकने पर हिला सकते थे। यह असुरक्षित दृष्टिकोण पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर और अलग-थलग कर गया।
अस्वीकार और प्रॉक्सी नेटवर्क की नीति: समय के साथ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां समानांतर नेटवर्क चलाने में माहिर हो गईं — दुनिया के साथ सहयोग का नाटक करते हुए हथियारबंद गुटों का समर्थन करना शुरू कर दिया। जबकि इस्लामाबाद शांति का भागीदार बनने का दावा करता था, उसके कार्य अक्सर इसके विपरीत थे। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और आधिकारिक गवाहियां पाकिस्तान के दोहरे खेल को उजागर करती हैं — विदेशी सहायता लेते हुए उन समूहों को आश्रय देना जो क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करते थे।
2021 का पल: जब पाकिस्तान के प्रॉक्सी उसके ही खिलाफ हो गए
टीटीपी का प्रतिशोध: पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ दानव
तालिबान के कब्जे के बाद, पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि वे उस तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने पाकिस्तानी नागरिकों और सैनिकों पर हजारों हमले किए। इसके विपरीत, पाकिस्तान में टीटीपी के ऑपरेशन बढ़ गए, और लड़ाके अफगान क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं।
यह अनुमानित था क्योंकि पाकिस्तान ने वर्षों तक जिहादी नेटवर्कों का समर्थन, सशस्त्र समूहों का प्रशिक्षण, और अत्याचार को बढ़ावा दिया। टीटीपी का इतिहास और विचारधारा तालिबान से जुड़ी हुई हैं — यानी पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ दानव जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता।
तालिबान नेताओं ने, जिसमें कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब भी शामिल हैं, पाकिस्तान की मांगों को ठुकरा दिया और मध्यस्थता की जो भी कोशिशें कीं, बार-बार विफल रही।
डुरंड लाइन विवाद
पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि तालिबान डुरंड लाइन को वैध सीमा के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके विपरीत तालिबान ने अफगानिस्तान की ऐतिहासिक स्थिति का समर्थन करते हुए इसे ठुकरा दिया और कह दिया कि यह सीमा उपनिवेशवादी है। तालिबान का यह अस्वीकार पाकिस्तान की ख़राब छवि और अफगान राष्ट्रवाद को उजागर करता है। तालिबान के नेता ख़ैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्रों को ऐतिहासिक रूप से अफगानी जमीन मानते हैं।
कूटनीतिक टूट
पाकिस्तान की उम्मीद थी कि तालिबान पाकिस्तान के आश्रित राज्य के रूप में काम करेंगे, सुरक्षा और कूटनीति में इस्लामाबाद का नेतृत्व मानेंगे। इसके उलट, तालिबान पूरी स्वतंत्रता का दावा करते हैं और अक्सर पाकिस्तान को दरकिनार करते हैं। सीमा संघर्ष आम हो गए हैं, लोग हताहत हुए हैं, और कूटनीतिक प्रयास विफल रहे हैं।
सबक: पाकिस्तान ने तालिबान का गलत आंकलन किया। जो आश्रित था, वह स्वतंत्र बन गया और पाकिस्तान उन चरमपंथी नेटवर्कों के सामने उजागर हो गया जिन्हें उसने खुद विकसित किया था।
क्यों पाकिस्तान की रणनीति फेल हुई: गहराई से विश्लेषण
- नियंत्रण खोना
पाकिस्तान को लगा कि वह तालिबान को सप्लाई लाइन, सुरक्षित ठिकानों और कूटनीतिक चैनलों से नियंत्रित कर सकता है। यह तब काम करता था जब तालिबान नाटो से लड़ रहे थे, लेकिन काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद यह सब खत्म हो गया।
अब तालिबान सीधे चीन, रूस, ईरान, और केंद्रीय एशियाई देशों के साथ सौदे कर रहे हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ पड़ोसी है — और परेशान करने वाला पड़ोसी। - विचारधारा = वफादारी नहीं
पाकिस्तान को लगा कि तालिबान धार्मिक रूप से रूढ़िवादी हैं, इसलिए वे अपने आप पाकिस्तान के पक्ष में होंगे। यह बड़ी गलती थी।
तालिबान पश्तून राष्ट्रवाद, अफगान संप्रभुता और विदेशी नियंत्रण के विरोध को महत्व देते हैं। उनका रूढ़िवाद इस्लामाबाद के आदेश मानने का संकेत नहीं देता। - टीटीपी को कम आंकना
पाकिस्तान ने सोचा कि तालिबान टीटीपी को दबा देंगे। ऐसा नहीं है। टीटीपी की घनिष्ठ पारिवारिक और नजदीकी संबंध तालिबान के साथ हैं।
तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ सौदेबाजी के हथियार के रूप में देखते हैं। - वैकल्पिक योजना नहीं
पाकिस्तान ने सभी रणनीतिक अंडे तालिबान की टोकरी में रख दिए और गलत होने पर कोई वैकल्पिक योजना नहीं बनाई। अब, जब रिश्ता बिगड़ा है, इस्लामाबाद अलग-थलग है।
क्षेत्रीय प्रभाव: पाकिस्तान की हानि, अन्य का अवसर
भारत को रणनीतिक अवसर
तालिबान-पाकिस्तान झगड़े ने भारत को अप्रत्याशित मौका दिया। भारत ने कूटनीतिक चैनल खोले रखे, मानवीय सहायता दी, और काबुल में अपनी कूटनीतिक गतिविधियां जारी रखीं।
भारत का दृष्टिकोण विकास और मानवीय सहायता पर केंद्रित है, जबकि पाकिस्तान दशकों से हथियारबंद समूहों के समर्थन पर निर्भर है। परिणामस्वरूप, भारत की नीति पाकिस्तान की रणनीति से कहीं अधिक सफल और प्रभावी साबित हुई है।
चीन की बढ़ती चिंता
चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर करती हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव इन निवेशों को खतरे में डाल रहा है और चीनी कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता पैदा कर रहा है।
रिपोर्टों के अनुसार, बीजिंग ने दोनों पक्षों पर समझौता करने के लिए दबाव डाला, लेकिन सीमित सफलता ही मिली। चीन की नाराजगी पाकिस्तान की तालिबान के साथ संबंध प्रबंधन में असफलता के कारण बढ़ रही है, जिससे पाकिस्तान को एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानने में चीन को संदेह हो रहा है। इसके अलावा, चीन अब यह भी महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान का चरमपंथ का गढ़ होने का नाम उसके निवेश और कर्मचारियों के लिए जोखिम पैदा करता है।
आर्थिक व्यवधान
सीमा बंद और व्यापार प्रतिबंध दोनों अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान केंद्रीय एशियाई बाजारों तक पहुंच खो रहा है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बंदरगाहों तक पहुंच खो रहा है।
विश्व स्तर पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता की समस्या
जब पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ शिकायत करता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सहानुभूति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का स्वयं का रिकॉर्ड कि उसने दशकों तक अपने क्षेत्र से इन समूहों का समर्थन किया, पूरी तरह से जाना-पहचाना है। जब इस्लामाबाद टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है, तो अन्य देश आमतौर पर प्रतिक्रिया देते हैं: “आपने यह समस्या खुद पैदा की, इन चरमपंथी नेटवर्कों का दशकों तक समर्थन करके।”
अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों ने बार-बार पाकिस्तान की भूमिका को दस्तावेजीकृत किया है — जैसे कि क्वेटा और पेशावर में तालिबान नेताओं को आश्रय देना, जनजातीय क्षेत्रों और शहरों में प्रशिक्षण शिविर चलाना, और सशस्त्र समूहों को रणनीतिक गहराई प्रदान करना। वर्तमान संकट जिसे पाकिस्तान झेल रहा है, उसे आमतौर पर स्वयं-निर्मित माना जाता है, न कि किसी मासूम देश पर अचानक घटित हुआ कोई हादसा।
पाकिस्तान की चरमपंथियों के लिए सुरक्षित आश्रय देने वाली छवि मजबूती से स्थापित हो चुकी है। यह विश्वसनीयता की समस्या इस्लामाबाद की कूटनीतिक क्षमता को सीमित करती है और अंतरराष्ट्रीय समर्थन को घटाती है। सरल शब्दों में, दुनिया ज्यादातर पाकिस्तान को ही जिम्मेदार मानती है, जिसने वह समस्या बनाई जिसे अब वह स्वयं शिकायत के रूप में पेश कर रहा है।
आगे क्या होगा: पाकिस्तान के कठिन विकल्प
1. सैन्य वृद्धि:
टीटीपी के ठिकानों पर अफगानिस्तान में हमले करना, जिससे तालिबान शासन के साथ खुली लड़ाई का जोखिम है। लेकिन अफगानिस्तान पर हमला या हस्तक्षेप करना व्यावहारिक विकल्प नहीं है — इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है, बड़ी हताहतियां हो सकती हैं, पूर्ण पैमाने पर युद्ध का खतरा है जिसे सेना और अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर सकती, और यह देश को राष्ट्रीय संकट में डाल सकता है।
2. वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना:
टीटीपी हमलों और तालिबान की अवज्ञा के साथ जीना और स्थिति को सीमा सुरक्षा को मजबूत करके नियंत्रित करने की कोशिश करना। देश के भीतर यह कमजोर दिखाई देता है और मूल समस्या को हल नहीं करता — वह समस्या जो पाकिस्तान ने इन नेटवर्कों का समर्थन करके खुद पैदा की थी।
3. वार्ता के माध्यम से समाधान खोजना:
तालिबान के साथ सौदेबाजी करना और टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के बदले कुछ रियायतें देना। लेकिन वास्तव में पाकिस्तान तालिबान को क्या दे सकता है? आर्थिक मदद: अर्थव्यवस्था संकट में है। पाकिस्तान पहले ही क्षेत्रीय अस्थिरता का स्रोत माना जाता है, इसलिए तालिबान के लिए इसके विकल्प सीमित हैं।
निष्कर्ष: चरमपंथ की कीमत
तालिबान–पाकिस्तान संबंधों का पतन सिर्फ सहयोगियों के बीच झगड़ा नहीं है — यह पाकिस्तान द्वारा दशकों तक चरमपंथ को विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का पूर्वानुमेय परिणाम है। लड़ाकों को आश्रय देकर, सशस्त्र नेटवर्कों का समर्थन करके और अपने क्षेत्र से चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देकर, पाकिस्तान ने उन ताकतों का निर्माण किया जो अब खुद उसे खतरा पैदा कर रही हैं।
क्षेत्रीय स्तर पर, अस्थिरता बढ़ रही है, मानवीय संकट गहरा रहा है, और भारत अफगानिस्तान के साथ सकारात्मक संबंधों के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के लिए सबक कड़ा है: राज्य-प्रायोजित चरमपंथ की भारी कीमत होती है, और इसके परिणाम अब दुखद रूप से स्पष्ट हो चुके हैं।
संबंधित लेख:
- भारत का रणनीतिक संतुलन नीति 2025: अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों का प्रबंधन और घरेलू राजनीति का इसके विदेश नीति पर असर।
- 2025 रूस-यूक्रेन युद्ध का विश्लेषण: नाटो, ट्रम्प: नाटो की भूमिका, ट्रंप और आगे के संभावित परिदृश्य—वैश्विक भू-राजनीति का भारत पर प्रभाव।
- अमेरिका की ऊर्जा और जलवायु कूटनीति: अमेरिका कैसे ऊर्जा और जलवायु को वैश्विक प्रभाव के लिए इस्तेमाल करता है, और भारत के दृष्टिकोण के लिए संदर्भ।
लेख पसंद आया?
हमारे मुख्य पृष्ठ पर जाएं और नई जानकारियों व अपडेट्स के लिए सदस्यता लें!